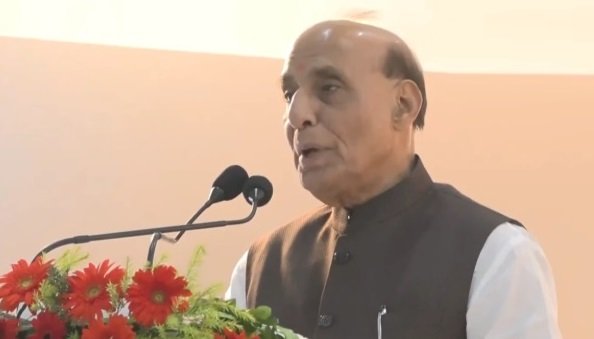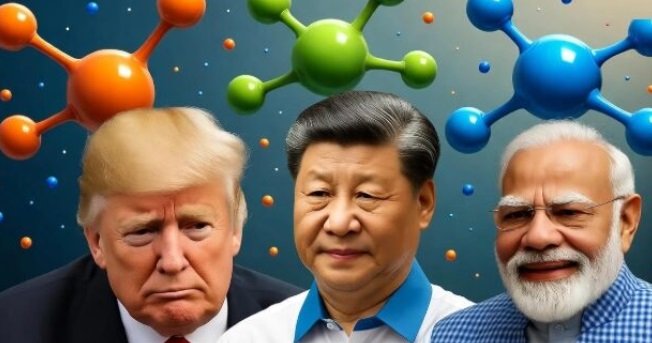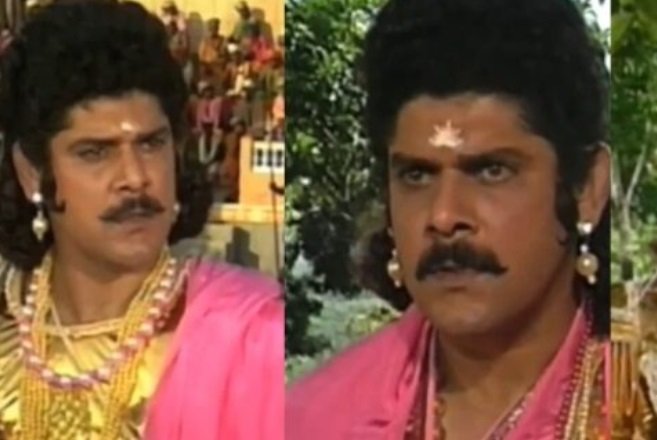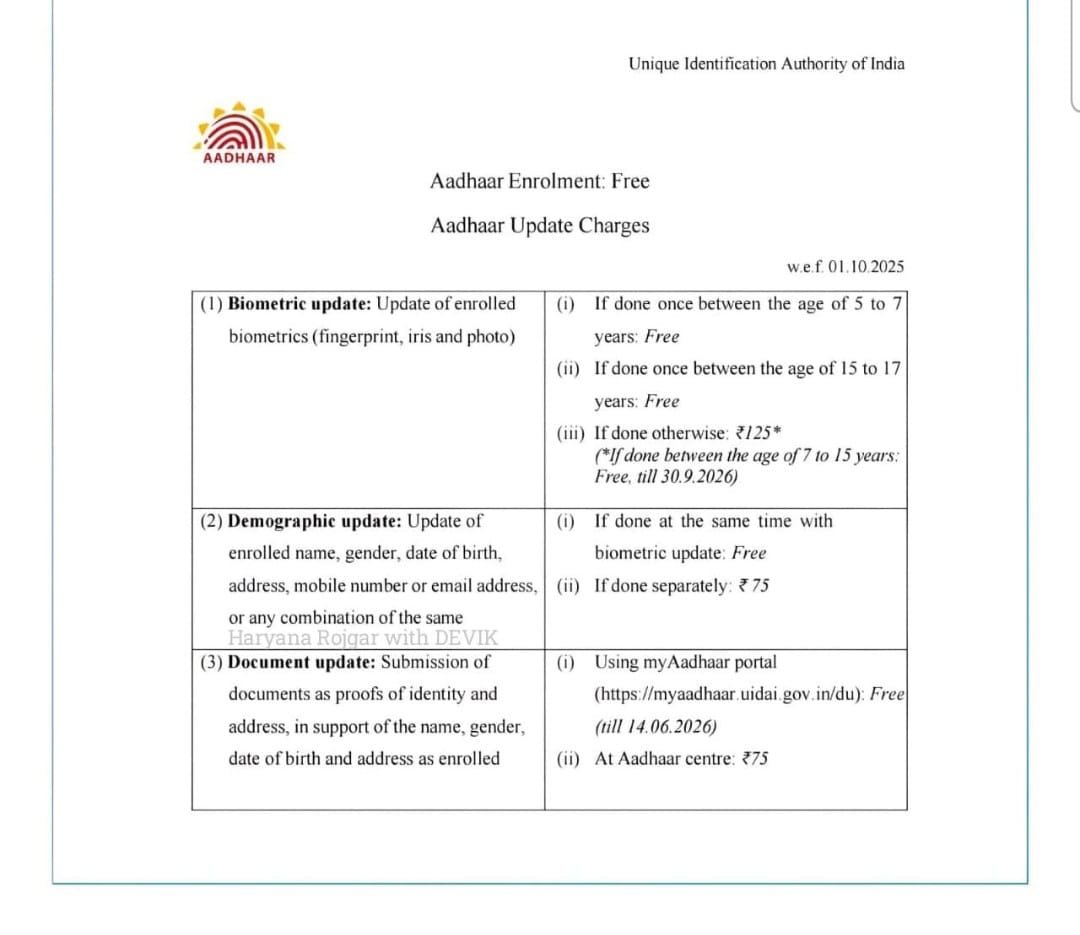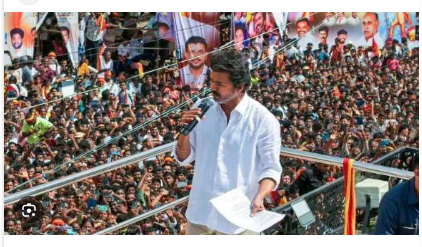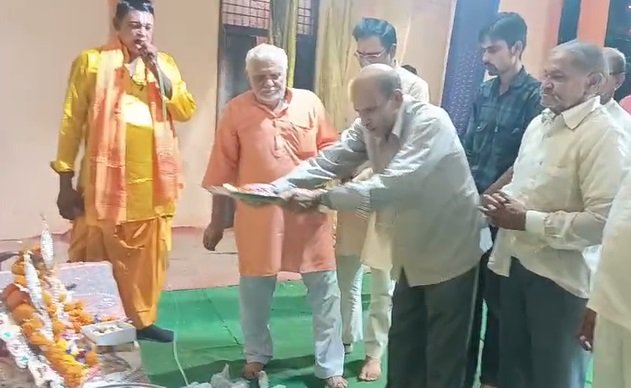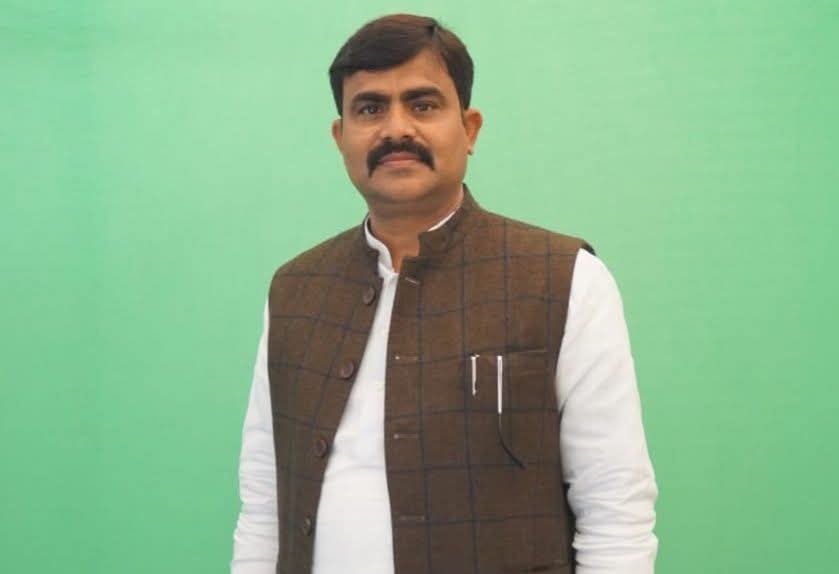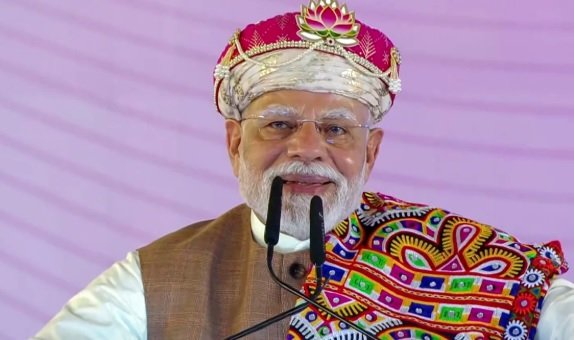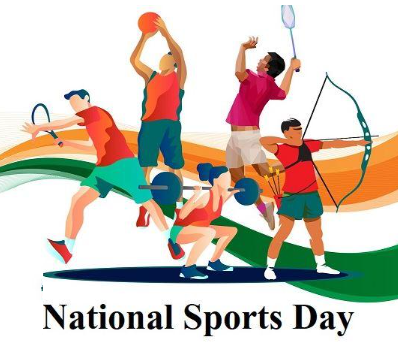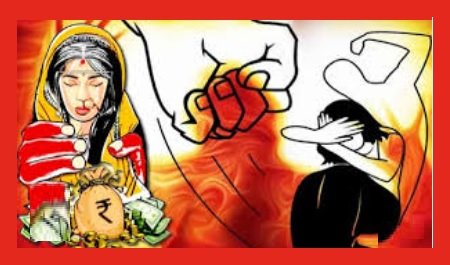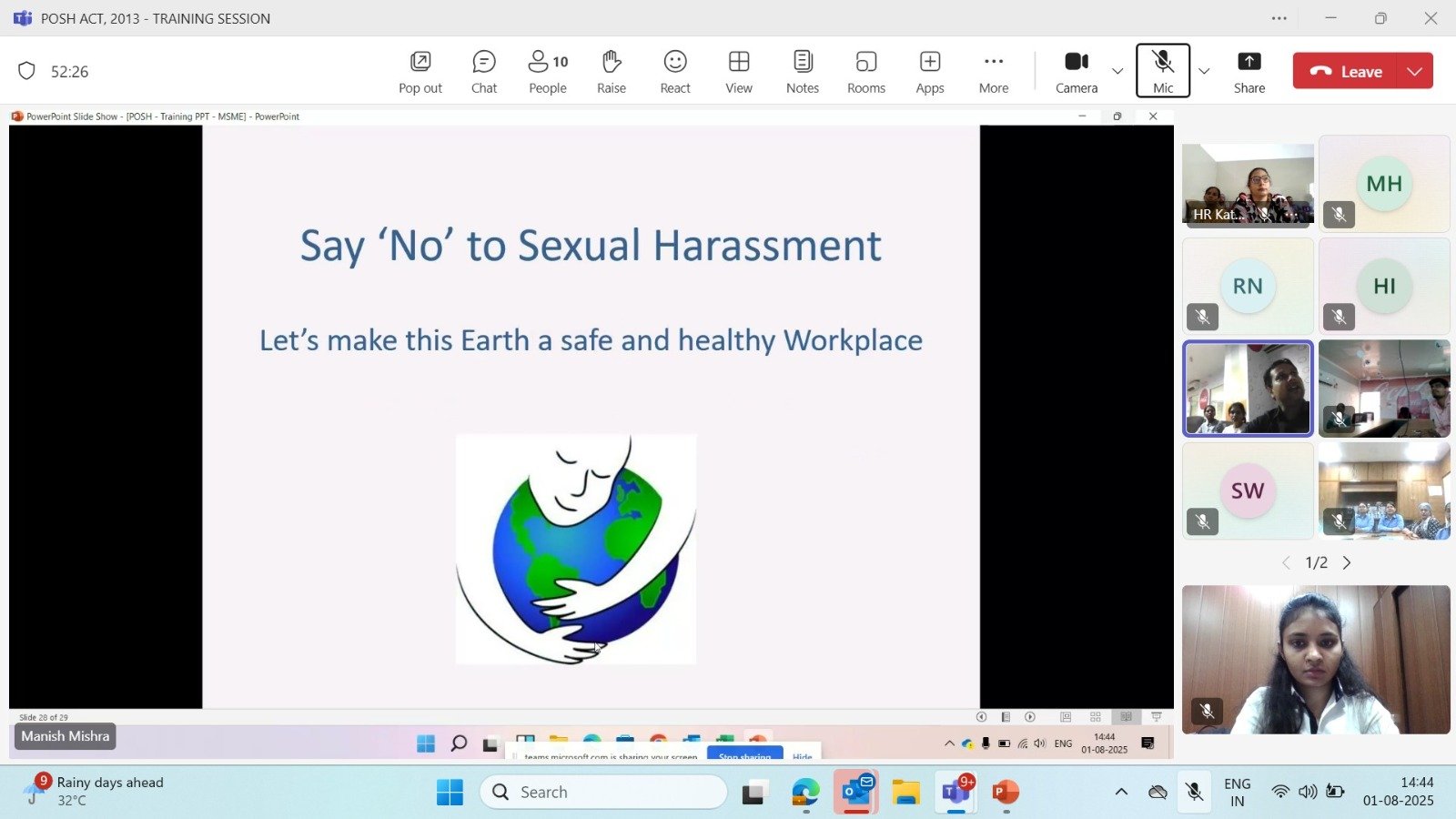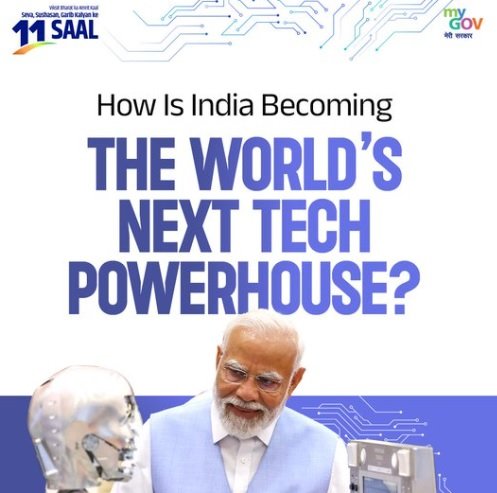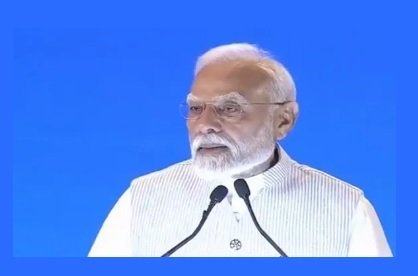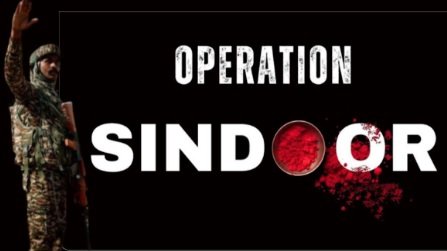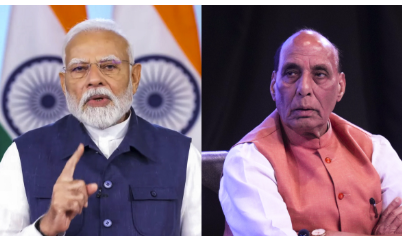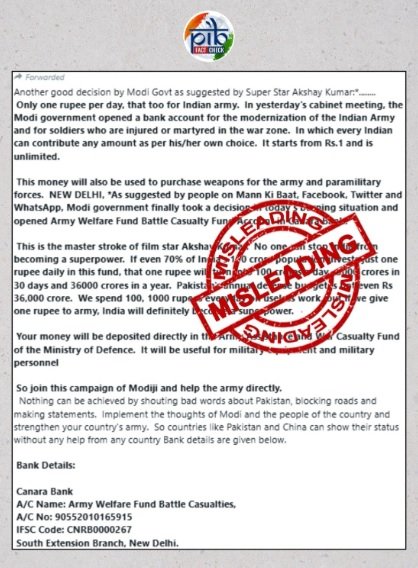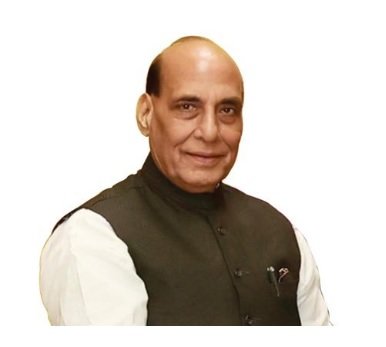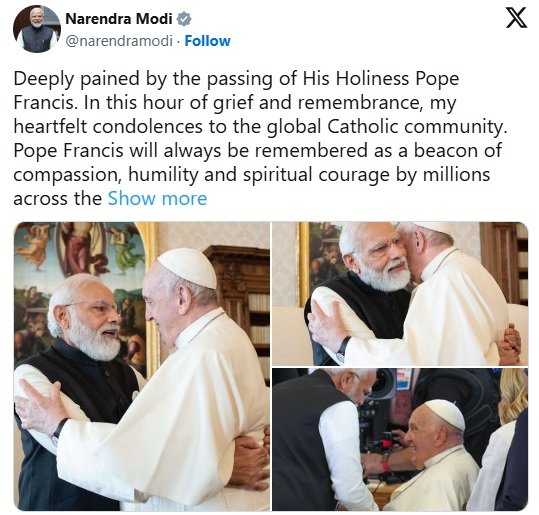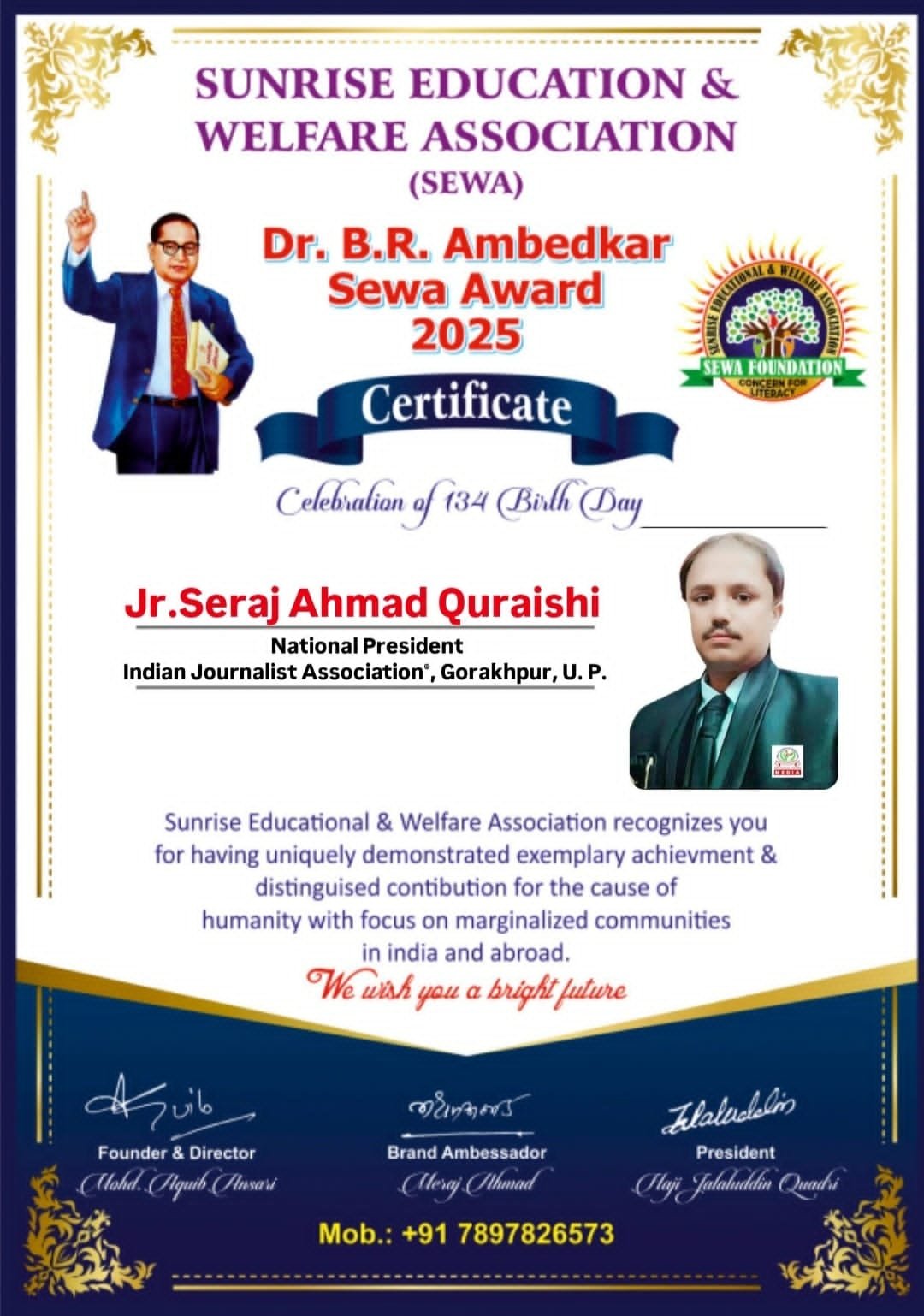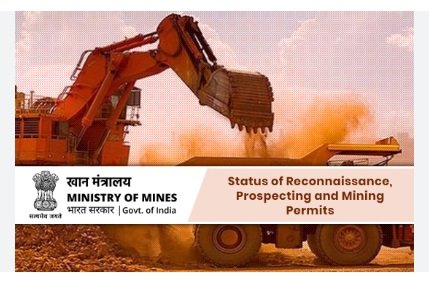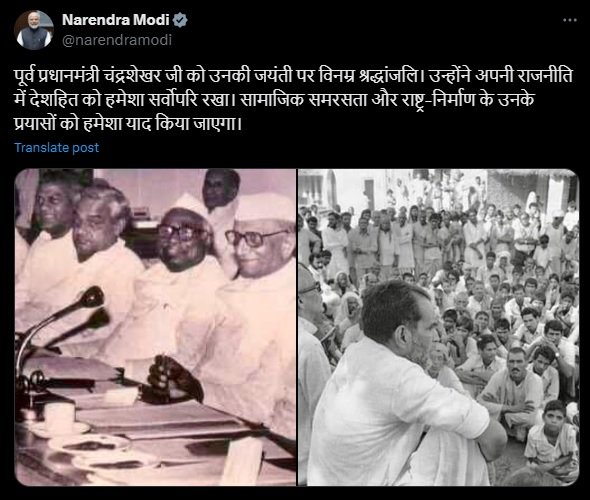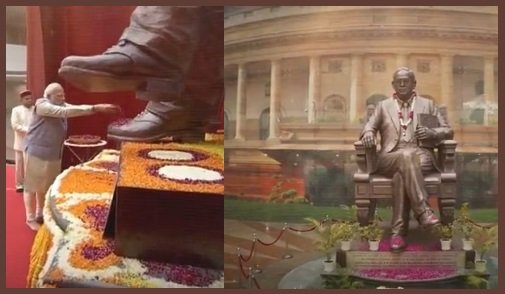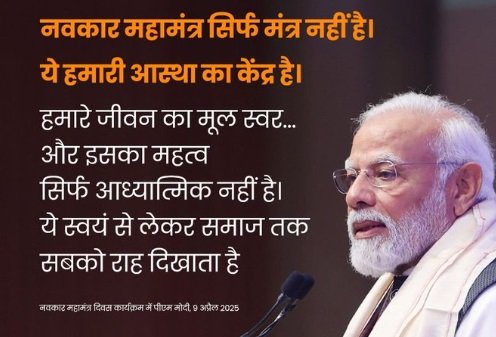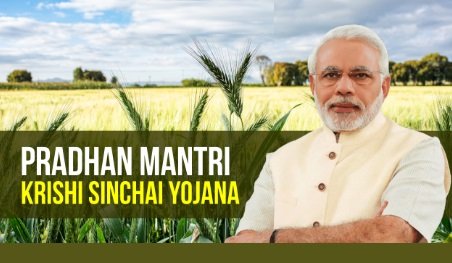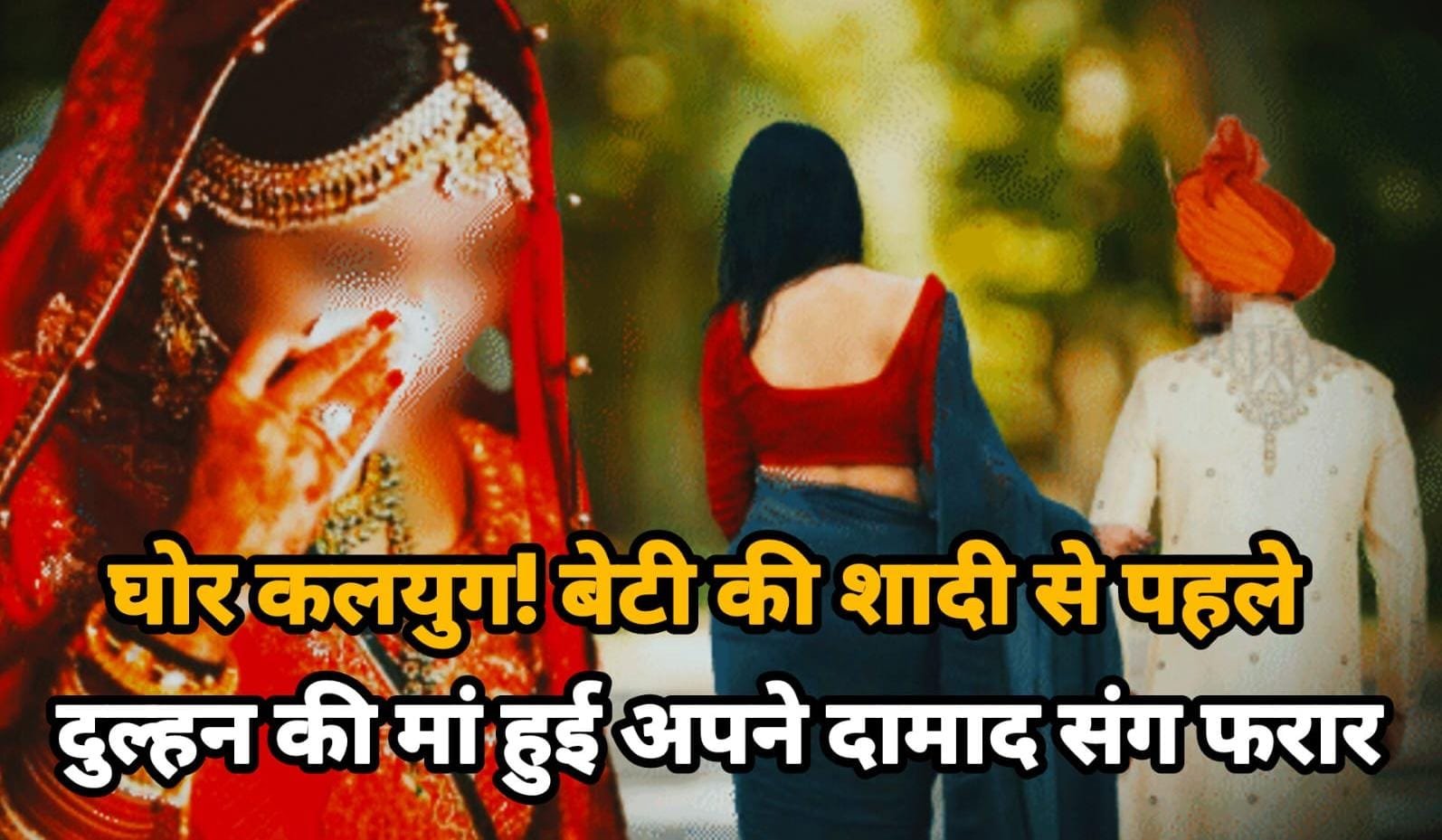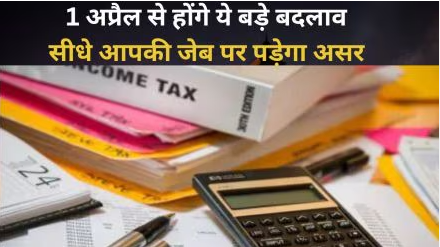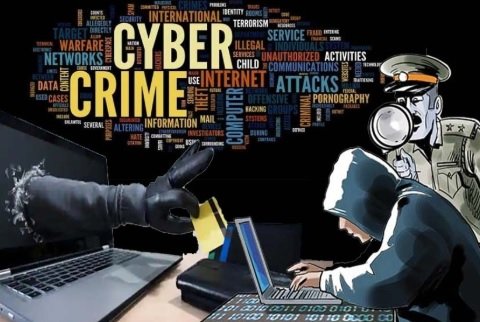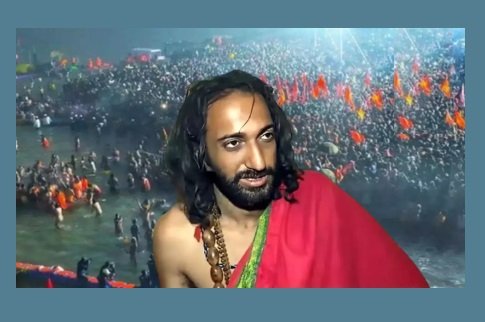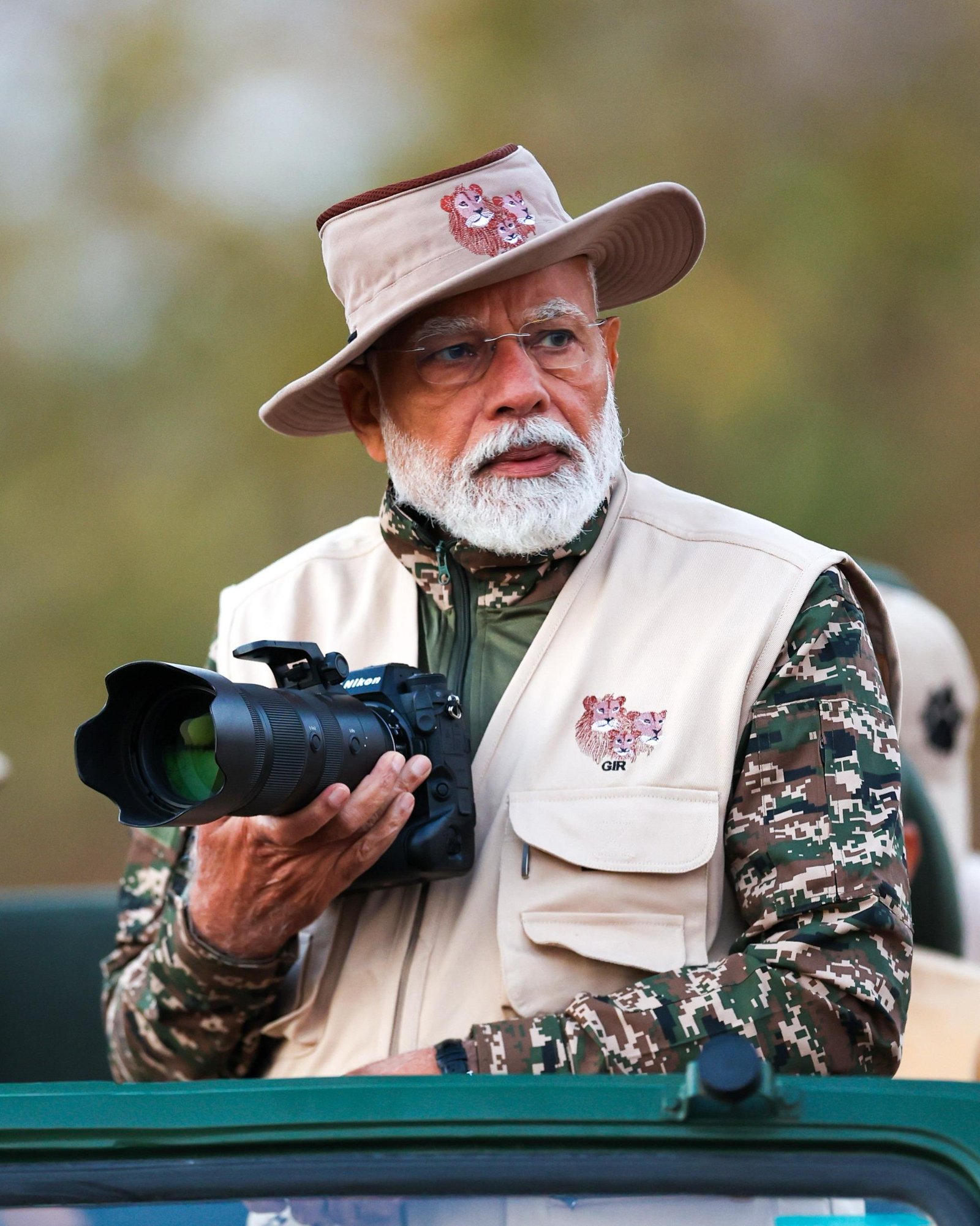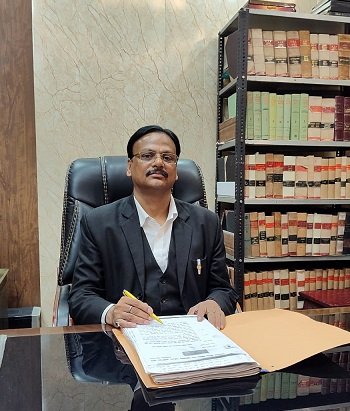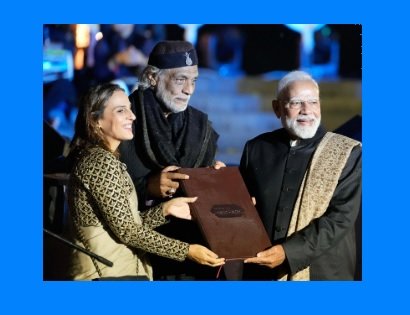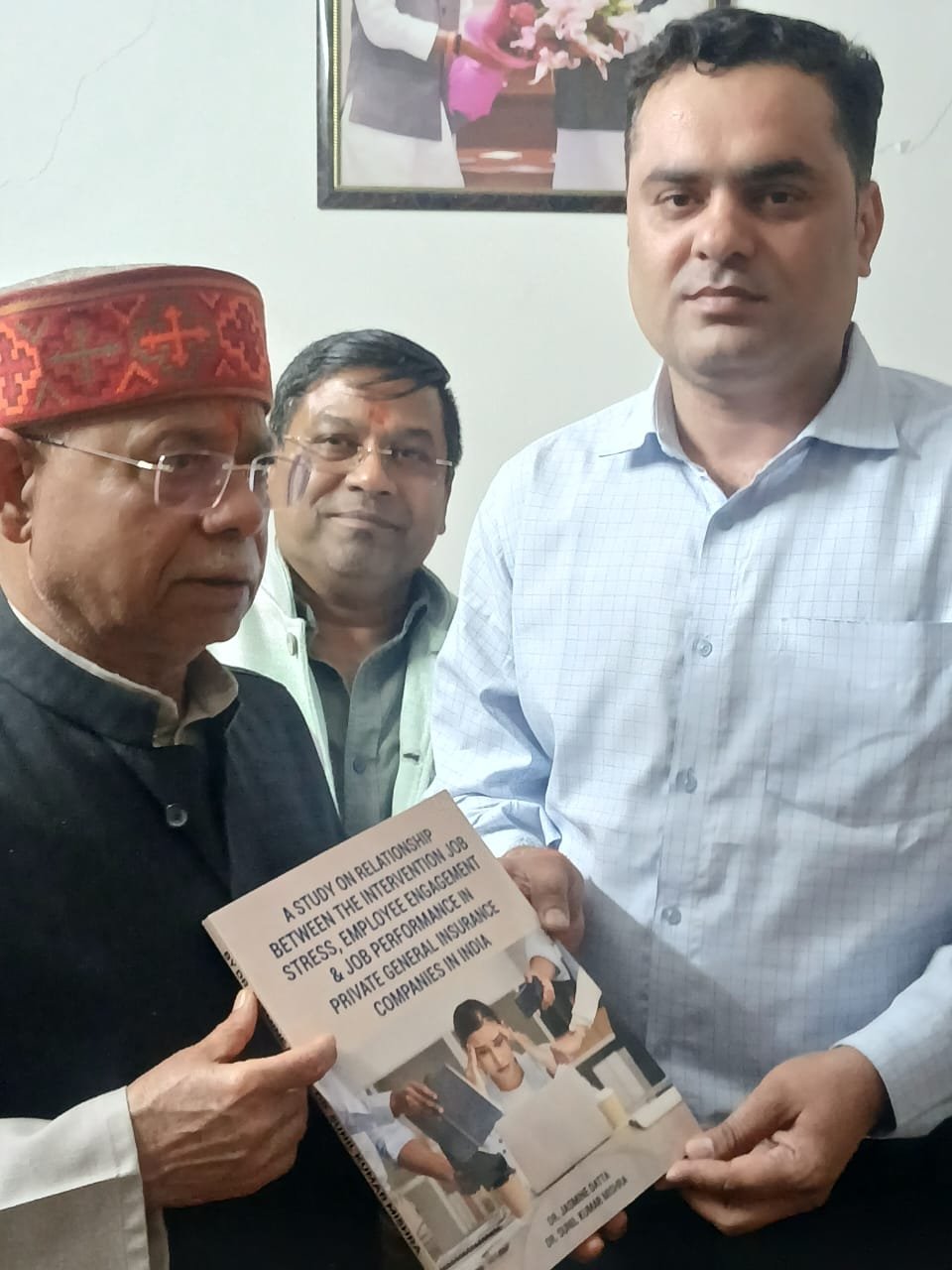14 सितम्बर, यह केवल एक तारीख़ नहीं, बल्कि हमारी राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़ा एक अवसर है। इस दिन 1949 में संविधान सभा ने हिंदी को देवनागरी लिपि में भारत की राजभाषा का दर्जा दिया था। तब से हर वर्ष यह दिन हमें यह स्मरण कराता है कि भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक पहचान और आत्मसम्मान की धुरी है। देखा जाये तो हर वर्ष 14 सितम्बर हमें यह याद दिलाने आता है कि भाषा केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक है। मगर यह भी सच्चाई है कि हिंदी को लेकर राजनीति का दौर कभी थमा नहीं। दक्षिण भारत से लेकर पूर्वोत्तर तक कुछ क्षेत्रीय दल समय-समय पर यह तर्क देते रहे हैं कि हिंदी को थोपने की कोशिश हो रही है। उनके लिए हिंदी का सवाल केवल भाषा का नहीं, बल्कि पहचान और अधिकार का भी है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या हिंदी का विरोध वास्तव में राष्ट्र के हित में है? हिंदी किसी पर थोपी नहीं जा रही, बल्कि यह स्वाभाविक रूप से करोड़ों भारतीयों की संपर्क भाषा बन चुकी है। रेलवे स्टेशन पर घोषणाएँ हों, फ़िल्मों के संवाद हों, या डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर सामग्री, हिंदी हर जगह मौजूद है और जनता की सहज पसंद बन चुकी है। विरोध करने वाले नेताओं को यह समझना चाहिए कि हिंदी को स्वीकार करना किसी क्षेत्रीय भाषा को कमज़ोर करना नहीं, बल्कि पूरे भारत को एक साझा सूत्र में पिरोना है।

हिंदी की ताक़त इसी में है कि यह संपर्क भाषा है। अंग्रेज़ी के सहारे संवाद करने की तुलना में हिंदी ज़्यादा आत्मीय और भारतीय परिवेश से जुड़ी हुई है। विश्व की 5वीं सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा होने के नाते यह केवल भारत की नहीं, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी पहचान बना रही है। यह भारतीय सिनेमा, साहित्य, पत्रकारिता और इंटरनेट की प्रमुख धुरी है।
राजनीतिक विरोध करने वालों को यह नहीं भूलना चाहिए कि स्वतंत्रता संग्राम के दौर में हिंदी ने जन-जागरण और राष्ट्र निर्माण में बड़ी भूमिका निभाई थी। महात्मा गांधी से लेकर सुभाषचंद्र बोस तक ने हिंदी को जनभाषा मानकर जनता से संवाद किया। यही कारण था कि संविधान सभा ने 14 सितम्बर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित कर राष्ट्रीय पहचान से जोड़ा।
आज जब हिंदी दिवस मनाया जा रहा है, तो उसका असली अर्थ यह है कि हम इस भाषा को केवल औपचारिकता से नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता के साधन के रूप में देखें। हिंदी किसी क्षेत्रीय भाषा की प्रतिस्पर्धी नहीं है, बल्कि वह सभी भारतीय भाषाओं को जोड़ने वाली सेतु है। इसलिए, हिंदी दिवस के मायने राजनीति से ऊपर उठकर समझने होंगे। विरोध करने वालों को यह समझना चाहिए कि हिंदी भारत की आत्मा है और आत्मा से विरोध राष्ट्र को कमज़ोर करता है। हिंदी का सम्मान करना किसी और भाषा का अपमान नहीं, बल्कि भारत की एकता और सांस्कृतिक शक्ति को मज़बूत करना है।
हिंदी केवल रोज़गार का साधन ही नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक शक्ति भी है। विश्वभर में जब भारतीय समुदाय अपनी भाषा में संवाद करता है, तो हिंदी भारतीय पहचान का दूत बन जाती है। संयुक्त राष्ट्र जैसे वैश्विक मंचों पर हिंदी की उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि यह केवल भारत तक सीमित नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय पटल पर भी प्रतिष्ठित हो रही है। भारतीय फ़िल्में और संगीत, जो दुनिया के कोने-कोने में लोकप्रिय हैं, उनकी मुख्य भाषा हिंदी ही है। यह न केवल भारत की सांस्कृतिक पहुँच को बढ़ाता है, बल्कि हमारी सॉफ्ट पावर को भी मज़बूत करता है।
वैसे, हिंदी का भविष्य तभी और सशक्त होगा जब हम इसे आधुनिक ज्ञान-विज्ञान और तकनीकी शब्दावली से समृद्ध करेंगे। शिक्षा संस्थानों में हिंदी माध्यम को रोजगारपरक बनाया जाए और शोध, विज्ञान, चिकित्सा तथा प्रौद्योगिकी की किताबें हिंदी में तैयार हों। यह भाषा तब सही मायनों में भारत का गौरव बनेगी, जब इसका प्रयोग केवल साहित्य या संवाद तक न रहकर जीवन और पेशेवर दुनिया के हर क्षेत्र में होगा।